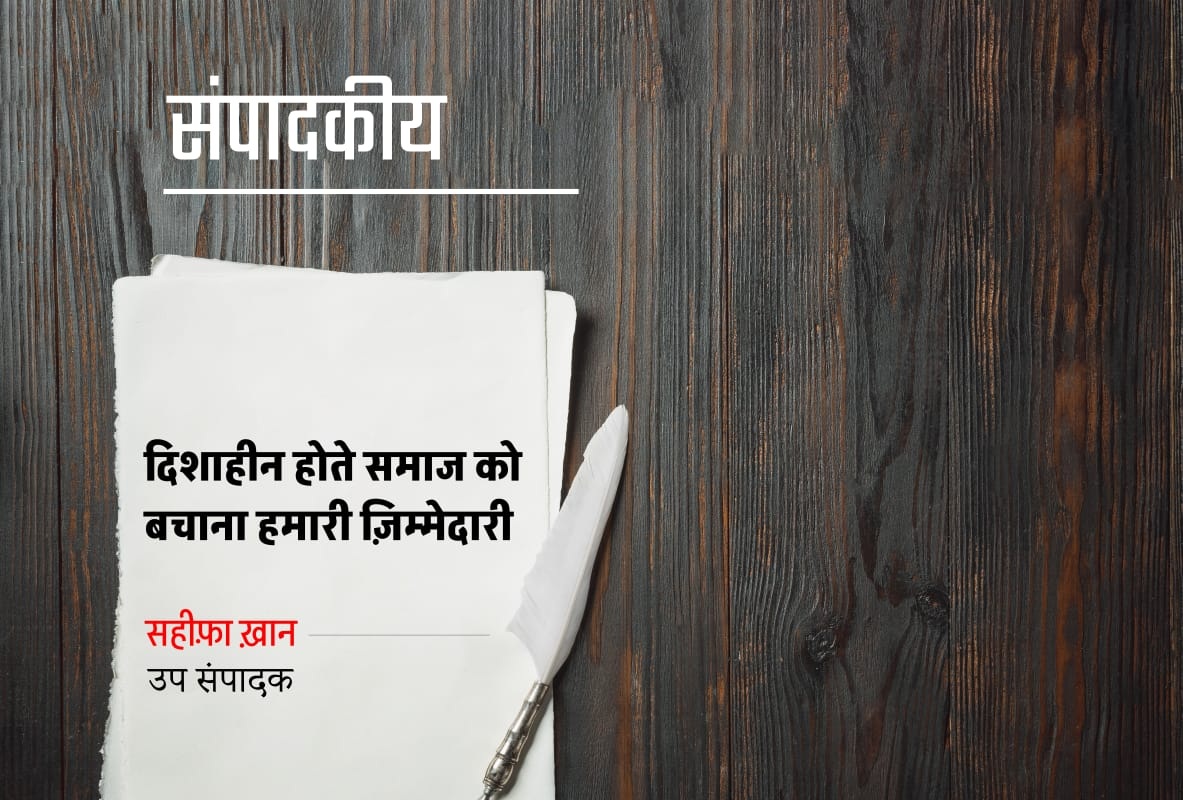मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी (रह०) की पुस्तक, शहादत इमाम हुसैन (रज़ि०), एम०एम०आई० पब्लिशर्स, नई दिल्ली से संकलित
हर साल करोड़ों मुसलमान मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन(रज़ि०) की शहादत पर अपने दुख और ग़म का इज़हार करते हैं लेकिन अफ़सोस है कि इनमें से बहुत ही कम लोग उस मक़सद पर ध्यान देते हैं जिसके लिए इमाम हुसैन ने न केवल यह कि अपनी प्यारी जान क़ुर्बान कर दी बल्कि अपने ख़ानदान के बच्चों तक को क़ुर्बान कर दिया। अगर यह शहादत किसी बड़े मक़सद के लिए नहीं होती तो सिर्फ़ निजी प्रेम और संबंध के कारण सदियों तक उसका दुख़ जारी रहने का कोई मतलब नहीं। और स्वयं इमाम हुसैन की अपनी नज़र में व्यक्तिगत और चरित्र प्रेम की क्या क़ीमत हो सकती थी। उन्हें अगर स्वयं का चरित्र उस उद्देश्य से ज़्यादा प्रिय होता तो वह उसे क़ुर्बान ही क्यों करते। उनकी यह क़ुर्बानी तो ख़ुद इस बात का सुबूत है कि वह उस उद्देश्य को अपनी जान से बढ़कर चाहते थे।
अब हमें यह देखना चाहिए कि वह क्या मक़सद था जिसके लिए इमाम हुसैन (रज़ि०) ने अपनी जान की बाज़ी लगाई? दरअसल यज़ीद को उत्तराधिकारी के रुप में देखकर हज़रत इमाम हुसैन समझ गए थे कि इस्लामी शासन की प्रवृत्ति और उसके व्यवहार और उसके तंत्र में किसी बड़े परिवर्तन के संकेत हैं जिसे रोकने का प्रयास करना उनके अनुसार आवश्यक था, यहां तक की इसमें लड़ने की नौबत आ जाए तो वह उसे न केवल यह कि महत्वपूर्ण बल्कि फ़र्ज़ समझते थे।
वह परिवर्तन क्या था? इतिहास को गहराई से पढ़ने पर हमारे सामने आता है कि परिवर्तन की शुरुआत यज़ीद को उत्तराधिकारी बनाना फिर उसको हुकूमत सौंपना था। इससे बिगाड़ की जो शुरुआत हो रही थी वह इस्लामी सत्ता के संविधान उसकी प्रवृत्ति और उसके उद्देश्य का परिवर्तन था। इस परिवर्तन के परिणाम निस्संदेह उस समय तक सामने नहीं आए थे लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति गाड़ी की दिशा परिवर्तित होते ही यह जान लेता है कि अब उसका रास्ता बदल रहा है, वह आख़िरकार उसे कहां ले जाएगी। यही दिशा परिवर्तन था जिसे इमाम हुसैन ने देखा और गाड़ी को फिर से सही पटरी पर डालने के लिए अपनी जान लड़ा देने का फ़ैसला किया।
राजतंत्र की शुरुआत
इमाम हुसैन देख रहे थे कि ख़िलाफ़त के स्थान पर राजतंत्र की शुरुआत हो रही है क्योंकि राजकुमार या उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजतंत्र में हुआ करती है, इस्लामी सत्ता में नहीं, इस्लामी सत्ता में ख़लीफ़ा जनमत से चुना जाता है। यज़ीद को उत्तराधिकारी बनाए जाने के फ़ैसले से मुसलमानों में राजतंत्र की शुरुआत हो गई।
नेकी का हुकुम देने और बुराई से रोकने के काम का बंद होना
इस्लामी सत्ता का उद्देश्य ईश्वर की ज़मीन पर उन नेकियों की स्थापना और बढ़ावा देना था जो अल्लाह को पसंद हैं और बुराइयों को दबाना और मिटाना था। मगर राजतंत्र का रास्ता अपनाने के बाद सत्ता का उद्देश्य देशों को जीतना, लगान टैक्स और मालगुजारी वसूल करना और ऐशपरस्ती के सिवा कुछ ना रहा। सियासत से अख़लाक़ जुदा होने लगा, सत्ता पर काबिज़ लोग अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बजाय अपने आप से डराने लगे और लोगों के ईमान और ज़मीर को जगाने के बजाय बख़्शिशों का लालच देकर उन्हें ख़रीदने लगे।
मूलभूत सिद्धांत में परिवर्तनः-
इसी प्रकार मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तन होने लगा जो संक्षेप में इस प्रकार थे:-
पहला सिद्धांत यह था की सत्ता लोगों की आज़ाद राय और इच्छा से स्थापित हो, कोई व्यक्ति अपने निजी प्रयास से उसे हासिल न करे बल्कि जनमत और सलाह से अच्छे से अच्छे शासक को चुनकर शासन उसे सौंप दिया जाए। अब जो परिवर्तन आ रहा था उसमें सत्ता के लिए लोगों पर बेअत का दबाव बनाया जाने लगा था।
दूसरा सिद्धांत सामूहिक राय (शूरा के मशवरे) का था। इस्लामी शासन का यह नियम होता है कि सलाह या राय उन से लोगों ली जाती थी जिनके इल्म, परहेज़गारी और सही राय देने की ख़ूबी पर आम लोगों को भरोसा था। इसके लिए एक सलाहकार कमेटी बनाई जाती थी, जिसके मेंबर सच्चे और ईमानदार लोग होते थे। जिनसे उम्मीद थी कि वे हर मामले में अपनी शिक्षा, अनुभव एवं ज़मीर (अंतरात्मा) के मुताबिक़ ईमानदारी के साथ निडर होकर बिल्कुल सही राय देंगे। लेकिन शाही दौर की शुरुआत होते ही शूरा का यह तरीक़ा बदल दिया गया।
इस्लामी सिद्धांत का तीसरा नियम यह था कि लोगों को अपनी बात कहने और राय देने की पूरी आज़ादी हो, नेकी का हुकुम देने और बुराई से रोकने को इस्लाम ने मुसलमानों का हक़ ही नहीं बताया बल्कि फ़र्ज़ क़रार दिया।लेकिन बादशाही की तरफ़ जाते ही ज़ुबान और दिलों पर ताले डाल दिए गए। अब तरीक़ा यह हो गया कि अगर मुंह खोलो तो तारीफ़ के लिए खोलो वरना चुप रहो।
चौथा सिद्धांत इस तीसरे सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ था कि ख़लीफ़ा और उसकी हुकूमत, अल्लाह और आम जनता दोनों के सामने जवाबदेह है। लेकिन राजतंत्र आते ही जवाबदेह सत्ता की कल्पना समाप्त हो गयी। अल्लाह के सामने जवाब देने का ख़याल चाहे ज़बान पर रह गया हो मगर अमल में नहीं था। आम जनता को इस हक़ से वंचित कर दिया गया था।
पांचवा सिद्धांत यह था कि सरकारी ख़ज़ाना ख़ुदा का माल है और मुसलमानों की अमानत है, जिसमें कोई चीज़ ग़लत तरीक़े से दाख़िल नहीं होनी चाहिए और जिसमें से कोई चीज़ ग़लत रास्ते में ख़र्च नहीं होनी चाहिए। चारों ख़लीफ़ाओं ने इसी सिद्धांत पर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से चलकर दिखाया। मगर जब ख़िलाफ़त राजतंत्र में परिवर्तित होने लगी तो ख़ज़ाना ख़ुदा और मुसलमान का नहीं बल्कि बादशाह का माल हो गया। हर जायज़ और नाजायज़ रास्ते से उसमें दौलत आने लगी और बेरोक टोक ख़र्च होने लगी। किसी की हिम्मत न थी कि उसके हिसाब का सवाल उठा सके।
छठा सिद्धांत यह था की कोई भी अल्लाह के क़ानून से ऊपर नहीं है और न किसी को क़ानून की हद से बाहर जाकर काम करने का हक़ होना चाहिए। एक आम आदमी से लेकर देश के शासक तक के लिए एक ही क़ानून होना चाहिए और सब पर उसे बेलाग तरीक़े से लागू होना चाहिए। इंसाफ़ के मामले में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चारों ख़लीफ़ाओं ने इस उसूल पर भी बेहतरीन नमूना पेश किया। वे बादशाहों से ज़्यादा ताक़त रखने के बावजूद भी अल्लाह के क़ानून के पाबंद थे। लेकिन ख़िलाफ़त के राजतंत्र में परिवर्तित होते ही इस नियम को भी नज़रअंदाज़ कर दिया गया।
मुसलमानों में अधिकार और गरिमा के हिसाब से समानता का नियम था जिसे इस्लामी शासन में पूरी ताक़त के साथ स्थापित किया गया था। मुसलमानों के बीच जाति, देश, भाषा इत्यादि को लेकर कोई भेदभाव न था। लेकिन ख़िलाफ़त की जगह जब राजतंत्र आया तो गुटबाज़ी और संकीर्णता के शैतान हर तरफ़ सिर उठाने लगे। अरब और ग़ैर अरब में, क़बीले और क़बीले के बीच खींचातानी शुरू हो गई। इस्लामी मिल्लत को इस चीज़ ने जो नुक़सान पहुंचाया उस पर इतिहास के पन्ने गवाह हैं।
इमाम हुसैन का मोमिनाना व्यक्तित्व
यह था वह परिवर्तन जो इस्लामी ख़िलाफ़त के राजतंत्र में परिवर्तित होने से सामने आया। कोई भी इस वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकता कि यज़ीद की सत्ता इन परिवर्तन की शुरुआत थी और इस बात से भी इनकार संभव नहीं है कि इस बिंदु से चलकर थोड़े ही समय के अंदर ही राजतंत्र में वह ख़राबियां साफ़ तौर पर दिखाई देने लगीं जो ऊपर बयान की गई हैं। जिस समय यह क़दम उठाया गया था उस समय यह ख़राबी पूरी तरह सामने नहीं आई थी मगर हर सोचने समझने वाला आदमी जान सकता था कि इसका नतीजा यही कुछ होने वाला है।
इमाम हुसैन (रज़ि०) ने इस चीज़ को महसूस किया इसीलिए उन्होंने यज़ीद के हाथ पर बेअत नहीं की और उन्होंने फ़ैसला किया कि जो बुरे से बुरा नतीजा भी उन्हें एक मज़बूत और जमी जमाई सत्ता के विरुद्ध उठने में भुगतना पड़े, उसका ख़तरा मोल लेकर भी उन्हें इसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश का जो अंजाम हुआ वह सबके सामने है मगर इमाम हुसैन(रज़ि०) ने इस बड़े ख़तरे में कूद कर और पूरी बहादुरी से उसके नतीजे झेलकर जो बात साबित की वह यह थी कि इस्लामी शासन के मूलभूत सिद्धांत मुस्लिम उम्मत की वह क़ीमती पूंजी है जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सिर भी दे दे और अपने बाल बच्चों को भी क़ुर्बान करदे, तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है।
इन विशेषताओं के मुक़ाबले में वे परिवर्तन जिन्हें ऊपर बयान किया गया है, दीन और मिल्लत के लिए ऐसी बड़ी आफ़तें हैं जिन्हें रोकने के लिए एक मोमिन को अगर अपना सब कुछ क़ुर्बान करना पड़े तो इसमें उसे चूकना नहीं चाहिए। किसी का दिल चाहे तो वह इसे एक ‘राजनीति’ काम कहले मगर हज़रत अली(रज़ि०) के बेटे हज़रत हुसैन(रज़ि०) की नज़र में तो यह सारासर एक ‘दीनी’ काम था, इसलिए उन्होंने इस काम में जान देने को शहादत समझ कर जान दी।
सैयदा हुमैरा, दिल्ली