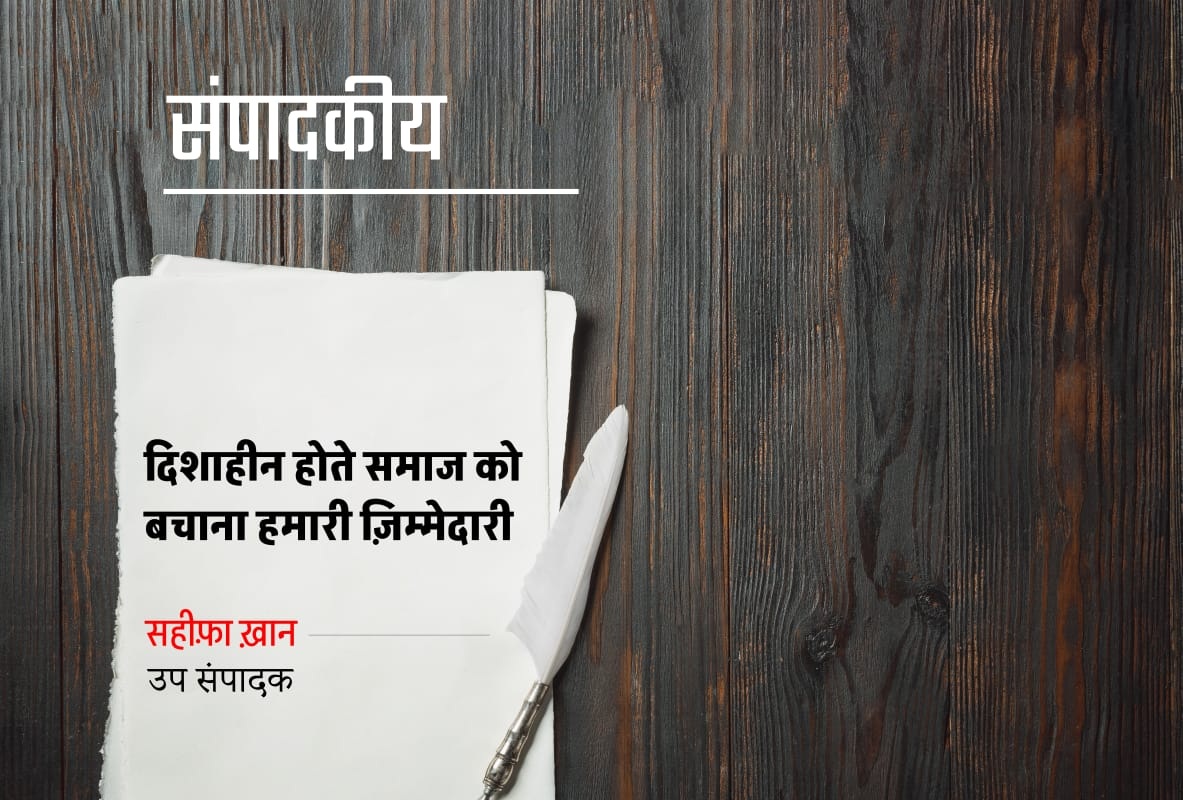स्वतंत्रता के 75 सालों बाद भी भारतीय समाज संविधान, स्वतंत्रता और समानता के विचार से ख़ुद को कितना जोड़ सका है यह भारतीय मीडिया के रुख को देखकर समझा जा सकता है। मीडिया का सामंतवादी और स्त्री विरोधी चेहरा (विशेषरुप से मुस्लिम महिलाओं को लेकर) समय-समय पर उसकी रिपोर्ट में साफ़ और स्पष्ट दिखाई देता है। हालांकि, कभी राष्ट्रवाद की आड़ में तो कभी धर्म आधारित सत्ता की आड़ लिए किसी विशेष नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मीडिया देश और समाज का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करता है।
वर्तमान में भारतीय मुख्यधारा मीडिया का बर्ताव उस व्यापक सामाजिक अन्याय की ओर भी संकेत करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की पहचान को संकुचित और दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में मीडिया की ज़िम्मेदारी इस से अधिक होनी चाहिए।
भारतीय मीडिया में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से रूढ़िगत छवियों में कैद रहा है। उन्हें अक्सर पर्दा या बुर्का पहनने वाली, शिक्षा से वंचित, धार्मिक बंदिशों में जकड़ी और पुरुष-प्रधान समाज की शिकार के रूप में दिखाया जाता है। यह छवि न केवल अधूरी है, बल्कि उस व्यापक विविधता और संघर्षशीलता को भी नकारती है जो मुस्लिम महिलाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
विशेषकर ट्रिपल तलाक, हिजाब विवाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों में मीडिया की भूमिका एक पक्षीय और सनसनीखेज़ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मीडिया द्वारा मुस्लिम महिलाओं की वास्तविक आवाज़ की जगह 'राजनीतिक एजेंडा' को प्राथमिकता दी गई है।
भारतीय मुख्यधारा मीडिया मुस्लिम महिलाओं को अक्सर 'पीड़िता' के फ्रेम में डाल देता है या फिर 'पर्दे के पीछे छुपी हुई महिला' के रूप में चित्रित करता है। वहीं दूसरी ओर हज़ारों मुस्लिम महिलाएं अपने समुदाय और समाज में बदलाव की अगुवा बन रही हैं, समाज के मुख्यधारा से जुड़कर सकारत्मक बदलाव के लिए काम कर रही हैं लेकिन मीडिया उन मुस्लिम महिलाओं की इन उपलब्धियों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर देता है। शायद एक पर्दा मीडिया के एक वर्ग की आँखों पर भी पड़ा है जिस से कि वह मुस्लिम महिलाओं के योगदान को देख नहीं पाता। जब तक मीडिया मुस्लिम महिलाओं की सफलता की कहानियों को ईमानदारी से दिखाना नहीं सीखेगा, तब तक उसका विमर्श अधूरा और पक्षपाती ही बना रहेगा।
भारत का पहला गैर-राजनीतिक और संविधान रक्षा आंदोलन मुस्लिम महिलाओं ने दिल्ली के शाहीन बाग़ से शुरू किया और देखते ही देखते यह देशभर में संविधान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आंदोलन साबित हुआ। इस आंदोलन को हिजाब पहनने वाली महिलाओं ने ही शुरू किया और इसे आगे बढ़ाया जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस आंदोलन को मुस्लिम महिलाओं ने तो शुरू किया लेकिन इस आंदोलन की भाषा, शब्दावली, शब्दों का चयन संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना से प्रेरित था, और सबसे महत्वपूर्ण कि यह आंदोलन एक समावेशी आंदोलन था।
किसान आन्दोलन के शुरुआती दिनों में जब देशभर से दिल्ली आ रही किसान महिलाओं से मीडिया ने पूछा कि आप किस से प्रभावित हैं और क्यों लगता है कि आप अपने आंदोलन में सफल होंगी? और आप कि मांगे मानी जाएंगी? तो किसान महिलाओं ने कहा कि हम शाहीन बाग़ आंदोलन और उसकी आंदोलनकारी महिलाओं को अपना आदर्श मानते है और हमें पूरा भरोसा है कि हम आंदोलन में सफल होंगे। देश ने देखा कि एक लंबे संघर्ष के बाद कृषि क़ानून वापस हुआ।
शाहीन बाग़ आंदोलन देश और समाज के साथ-साथ मीडिया के लिए भी मुस्लिम महिलाओं की छवि को नए सिरे से समझने का यह अवसर था, लेकिन मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इस अवसर को भी मुस्लिम महिलाओं की छवि पर आरोप लगाने, उनका चरित्रहनन करने, उन्हें पैसा लेकर धरने पर बैठने, बिरयानी के लिए धरने में शामिल होने का आरोप लगा कर इस आंदोलन और ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के अभियान में लगा दिया।
एक वर्ग को बुर्क़े और नक़ाब में मुस्लिम महिलाएं कुछ न कर पाने वाली और हाशिए पर रहने वाली प्रतीत होती हैं लेकिन वही नक़ाब पहनने वाली मुस्लिम माहिलाएं जब अपने अधिकारों के लिए और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरती हैं तो दुर्भावना से ग्रस्त मीडिया उस आंदोलन को बदनाम करने की मुहिम में लग जाता है या अपनी ख़बरों में इन पहलुओं को उजागर नहीं करता।
इसके लिए सभी तरीके और हथकंडे अपनाए जाते हैं। भारतीय मीडिया यह अच्छी तरह जानता है कि हमेशा किसी के विरोध में रिपोर्ट लिखना ही विरोध का तरीका नहीं होता बल्कि कभी या अक्सर मुद्दों को जगह न देना, विमर्श में न लाना और उन्हें मीडिया संस्थानों में चर्चा का विषय ही न बनाना भी विरोध का तरीका होता है और भारतीय मीडिया ये काम बहुत ही ज़िम्मेदारी से कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि दक्षिणपंथी रुख रखने वाले या सरकार समर्थित मीडिया चैनलों ने ही ऐसा किया है बल्कि सबसे पहले कोरोना पर धर्म विशेष यानि मुसलमानों के नाम की मुहर लगाने का काम दि हिन्दू जैसे सेक्युलर अख़बार ने किया है।
दो वर्ष पूर्व बीबीसी ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर की वीडियो स्टोरी प्रकाशित की थी जो 10 रुपये में मरीज़ों का इलाज करती है। आंधप्रदेश के कुडपा कस्बे की डॉक्टर नूरी परवीन जो MBBS डॉक्टर हैं और मात्र 10 रुपए में मरीज़ों की सेवा करती आ रही हैं। BBC ने उस मुस्लिम डॉक्टर महिला की तारीफ़ करते हुए मानवता की सेवा कह कर प्रशंसा की। हालांकि मुस्लिम महिला द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय कार्य में उसके धर्म इस्लाम का नाम नहीं लिया गया। वह मुस्लिम महिला अपने नाम से, कपड़ों से, अपने हिजाब से मुसलमान है और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्म से इस्लाम के विचारों पर चलते हुए यह सेवा कार्य कर रही है।
जो मीडिया कपड़ों और नामों से इस्लाम को तुरंत जोड़ देता है वह मीडिया किसी मुस्लिम महिला डॉक्टर द्वारा की जा रही जन सेवा को मानवता से जोड़कर आगे बढ़ जाता है। मुसलमानों द्वारा किये जा रहे बुरे काम को इस्लाम से जोड़ना और अच्छे काम को मानवता से जोड़ना कहाँ की पत्रकारिता है?
सकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा:
हिजाब मुद्दे को लेकर भारतीय मीडिया के एक बड़े वर्ग ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष को सामने लाने के बजाए एकतरफा और पक्षपाती रिपोर्टिग की और उन्हें हाशिए पर ला खड़ा किया। हालांकि भारत की मुस्लिम महिलाएं आज ग्राम पंचायत से लेकर वैश्विक मंच तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।
कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान, जिसने हिजाब पहनने के अधिकार के लिए साहसपूर्वक खड़ी होकर वैश्विक पहचान बनाई, या ज़मीनी स्तर पर कार्यरत हजारों महिलाएं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, ये सभी एक सशक्त छवि प्रस्तुत करती हैं।
लेकिन मुख्यधारा मीडिया इन कहानियों को न तो प्रमुखता से दिखाता है, न ही उनके पीछे के सामाजिक संघर्ष को समझने की कोशिश करता है। मीडिया की व्यावसायिक मजबूरियाँ, टीआरपी की होड़ और राजनीतिक गठजोड़ इस सकारात्मक विमर्श को अक्सर दबा देते हैं।
क्या है उपाय?
किसी समाज में जब मीडिया द्वारा किसी वर्ग या समुदाय को निशाना बनाया जाता है और उसके विरोध में नैरेटिव चलाया जाता है तो ऐसे समय में स्वयं उस वर्ग और समुदाय को आगे आकर उन्ही माध्यमों को अपनाकर अपना पक्ष रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस समय मीडिया में बतौर पत्रकार, एंकर, लेखक और संपादक मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही भारतीय पत्रकारिता को भी अपनी रिपोर्ट में इन्क्लूसिव और समावेशी होने की आवश्यकता है।
इसी क्रम में कम्युनिटी मीडिया का विस्तार भी आवश्यक है ताकि महिलाएं अपने मुद्दे, अपनी कहानियां अपनी भाषा में कह सके। मुस्लिम समुदाय के भीतर से खुद की आवाज़ उठाने वाले वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए। इसके साथ ही मीडिया हाउसेज़ को अपनी एडिटोरियल गाइडलाइन्स की समीक्षा भी करनी चाहिए ताकि किसी समुदाय विशेष के प्रति पूर्वग्रह न बढ़ाया जाए।
मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना चाहिए और कम्युनिटी मीडिया प्लेटफार्म पर उसे प्रकाशित करना चाहिए। यह हमें समझना होगा कि मीडिया में जब शोध और डेटा आधारित रिपोर्टिंग की जाती है तो इसका असर काफी दूर तक देखा जाता है और चर्चा का विषय बनता है।
अपनी कहानी ख़ुद कहना होगा:
मुस्लिम महिलाओं को एक 'समूह' की तरह देखने की प्रवृत्ति भी समस्या का हिस्सा है। उनके बीच भी वर्ग, क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा के विभिन्न स्तर हैं। एक ओर जहां उच्च शिक्षित, आधुनिक सोच वाली महिलाएं टेक्नोलॉजी, लॉ, मीडिया और प्रशासन में सफल हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भरता के लिए स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व कर रही हैं।
मीडिया की इस विविधता को समझने और दिखाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वह एक 'सांस्कृतिक प्रतीक' या 'राजनीतिक उपकरण' के रूप में मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल करे।
यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम महिलाओं की छवि का सवाल केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय मीडिया की लोकतांत्रिक जवाबदेही और सामाजिक समरसता की कसौटी है।
मुख्यधारा मीडिया को यह समझना होगा कि हर बार पर्दा या पीड़िता दिखाकर वह सिर्फ एक स्टीरियोटाइप को मज़बूत करता है, ज़बकि जमीनी हकीकत कुछ और है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जब तक मुख्यधारा मीडिया मुस्लिम महिलाओं की सफलता की कहानियों को उतनी ही ईमानदारी से दिखाना नहीं सीखेगा, तब तक उसका विमर्श अधूरा और पक्षपाती बना रहेगा और एक समुदाय विशेष को पीछे धकेलने की साज़िश सा प्रतीत होगा।
मसीहुज़्ज़मा अंसारी
संपादक, इंडिया टुमारो, नई दिल्ली